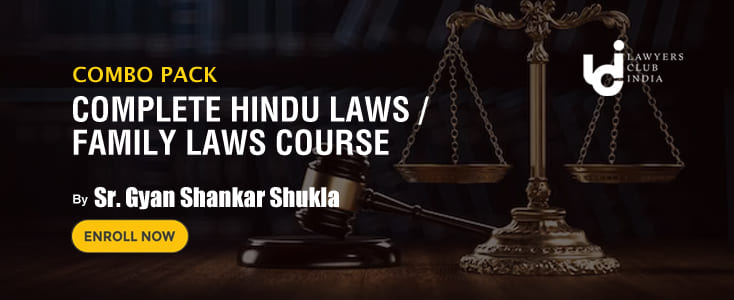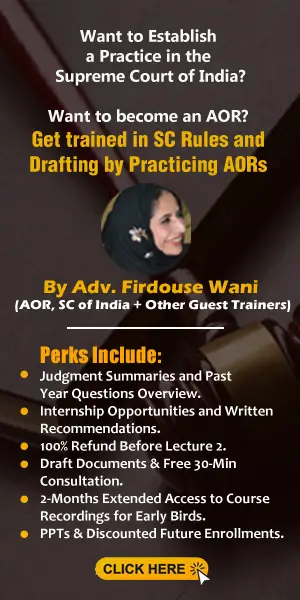दरिद्रता के गर्त में समाए हुए शहरी भारतीयों को मध्यवर्ग में रख कर केवल ग्रोथ के आंकड़ों को झूठ की पालिश लगा कर चमकाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत में आए समृद्धि के उछाल को इस तरह की कारिस्तानी की जरूरत है?
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की ताजा रपट ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि आमदनी के लिहाज से किसे मध्यवर्ग कहा जाना चाहिए। एडीबी कहता है कि दो डॉलर से लेकर बीस डॉलर प्रतिदिन खर्च कर सकने वाला व्यक्ति मध्यवर्ग की श्रेणी में आता है। उसके इस आकलन में भारत भी शामिल है।
बैंक की मान्यता है कि 1990 से 2008 के बीच भारत की आबादी में मध्यवर्ग का हिस्सा बीस करोड़ पचास लाख तक पहुंच चुका है। जहां तक बीस डॉलर का सवाल है, यह ऊपरी सीमा ठीक लगती है। मोटे तौर पर अगर एक डॉलर को पचास भारतीय रुपयों के बराबर मान लिया जाए, तो कहा जा सकता है कि जो लोग एक हजार रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकते हैं उन्हें मध्यवर्गीय समझने में कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन, जो लोग दो डॉलर से दस डॉलर के बीच यानी सौ रुपए से लेकर पांच सौ रुपए तक ही खर्च कर सकते हैं, उन्हें मध्यवर्गीय करार देना गले से नहीं उतरता। सवाल यह है कि इन लोगों को गरीब वर्ग की श्रेणी में क्यों नहीं डालना चाहिए? यह भी आकलन की एक विचित्र पद्धति है कि गरीब हम उन्हीं को मानें जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं या उसके ठीक ऊपर हैं।
तीन से लेकर पंद्रह हजार रुपए प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति का जीवन इस महंगाई के जमाने में हाथ से लेकर मुंह के बीच ही सीमित रहने के लिए अभिशप्त है। वह न तो शिक्षा के बारे में सोच सकता है, न ही स्वास्थ्य-रक्षा के बारे में। जबकि मध्यवर्ग होने की सर्वप्रमुख कसौटी यह है कि उसके पास पेट भरने, शरीर ढंकने और रिहाइश पर व्यय करने के बाद इतना जरूर बचना चाहिए कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से न केवल अपने वर्तमान को दुरुस्त कर सके, वरन भविष्य के लिए भी कुछ योजनाएं बना सके।
यह बहस उस समय और भी दिलचस्प हो जाती है जब हमारे आíथक टिप्पणीकार एडीबी की इस रपट की आलोचना न करके उसे एक मानक की तरह स्वीकार करते हैं। वे इस रपट को बिना प्रश्नांकित किए मान लेते हैं कि सौ रुपए रोज कमाने वाला भी मध्यवर्गीय है। इस परिभाषा के अनुसार तो शहरी अपार्टमेंटों में चौकीदारी करने वाले, घरों में काम करने वाली बाइयां, सफाई करके रोजी कमाने वाले, चपरासी, हरकारे, वजन ढोने वाले, रिक्शा खींचने वाले, खोमचे लगाने वाले और फेरी लगाने वाले शहरी गरीब मध्यवर्गीय हुए।
इन टिप्पणीकारों का रवैया उस समय हास्यास्पद हो जाता है जब वे भारत सरकार को सुझाव देते हैं कि उसे अपनी आíथक नीतियों में दो डॉलर रोज और उससे ज्यादा कमाने वाले लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे भावना यह निकलती है कि अगर सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर हो रहे उनके खर्च की जिम्मेदारी उठा लेगी, तो ये लोग वह रकम बचा लेंगे जो इस मद में जा रही है। बचत करके वे इस रकम को अपनी ‘फ्यूचर ग्रोथ’ में खपा सकेंगे।
आíथक विश्लेषण से जुड़ा यह बचकानापन कल्पनातीत है। दरिद्रता के गर्त में समाए हुए शहरी भारतीयों को मध्यवर्ग में रख कर केवल ग्रोथ के आंकड़ों को झूठ की पालिश लगा कर चमकाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत में आए समृद्धि के उछाल को इस तरह की कारिस्तानी की जरूरत है?
आखिर इस हकीकत को मान लेने में क्या हर्ज है कि जो लोग सौ रुपए रोज कमा रहे हैं और तकरीबन दिहाड़ी मजदूर की स्थिति में हैं, वे गरीबी की रेखा के नीचे से तो निकल आए हैं, पर उन्हें और ऊपर ले जाने के लिए उन्हें सरकार की विशेष नीतियों की आवश्यकता होगी। यह एक खास तरह की श्रेणी है जो पहला झटका लगते ही फिर से बीपीएल की हैसियत में पहुंच जाएंगे।
कहना न होगा कि ऐसे बहुत से लोगों को (कम से कम उन्हें जो सौ से ढाई सौ रुपए रोज कमाते हैं) असंगठित क्षेत्र में काम मिला हुआ है। इस श्रेणी का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। जो लोग इससे थोड़ा ऊपर हैं यानी ढाई से पांच-छह सौ रुपए रोज कमाते हैं, उन्हें सेवा क्षेत्र और निर्यातोन्मुख उत्पादन के क्षेत्र में निचले स्तर का रोजगार प्राप्त है।
यह क्षेत्र हमेशा बहुत नाजुक स्थिति से गुजरता रहता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैसे ही किसी सेवा की मांग घटती है या किसी उत्पाद के निर्यात-ऑर्डर मिलने कम हो जाते हैं, वैसे ही इन लोगों की छंटनी या ले-ऑफ का दौर शुरू हो जाता है। देखते-देखते नौकरियां हाथ से निकल जाती हैं और इन लोगों की हालत सौ रुपए रोज कमाने वालों जैसी या उनसे भी ज्यादा खराब होती नजर आती है। इसलिए इसे ‘वल्नरेबल मिडिल क्लास’ कहने के बजाय ‘वल्नरेबल लोअर क्लास’ कहना अधिक उचित होगा।
ऐसे लोग भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में फैले हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेती और खेती आधारित रोजगार का कबाड़ा हो जाने एवं सामाजिक सुरक्षा की पारंपरिक संरचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ये लोग पिछले पच्चीस-तीस सालों में शहरों का रुख करने को मजबूर हुए हैं। चाहे लातीनी अमेरिका के अर्जेटीना जैसे देश हों या दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश, हर जगह इनकी कहानी एक ही है।
शहरों में आने के बाद ये लोग खुद को किसी भी तरह के कौशल से वंचित महसूस करते हैं। इन्हें खुद को प्रशिक्षित करने में बहुत समय लगता है। संभवत: इनकी आधी या एक पूरी पीढ़ी इस प्रक्रिया में खुद को होम कर देती है। तब कहीं जाकर नई पीढ़ी मनोगत रूप से यह कल्पना करने में भी समर्थ होती है कि जिस निचले पायदान पर वह खड़ी है उससे ठीक ऊपर एक और पायदान है जिस पर उसे कदम रखना चाहिए। अगर वास्तव में इन लोगों को मध्यवर्ग की श्रेणी में फिट करना है, तो गांव से उजड़ कर शहर आने वालों के प्रति राजनेताओं और नीति निर्माताओं को अपनी दृष्टि में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा।
इन्हें खास तौर से लक्ष्य बना कर शहरी समाज और उत्पादन की औद्योगिक विधियों को आत्मसात करने के लिए विशेष सुरक्षा योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे। इसके लिए शहरी विकास की आधारभूत कल्पनाशीलता में परिवर्तन करना होगा। वरना होगा यह कि सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इन लोगों का उपयोग ग्रोथ के फर्जी आंकड़े बढ़ाने में करती रहेंगी। दूसरी तरफ ये लोग गरीब से अतिगरीब की श्रेणियों में दुर्भाग्यपूर्ण आवाजाही करते रहेंगे।